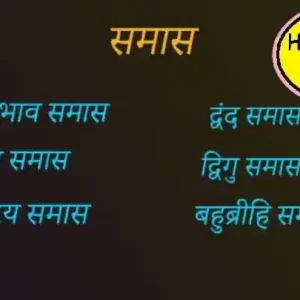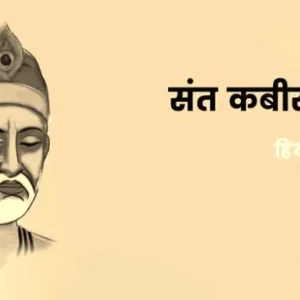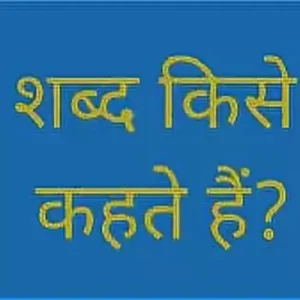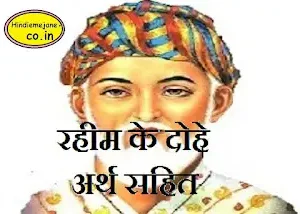Table of Contents
समास की परिभाषा
समास का अर्थ है ‘संक्षिप्तीकरण’ जब परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक स्वतन्त्र और सार्थक शब्द बनाते हैं तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं, जैसे-‘राजा का पुत्र’ का सामासिक पद होगा-‘राजपूत्र’। पदों को जोड़कर संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है और समास बनाने की इस प्रक्रिया में कारक-चिह्नों, परसर्गों और योजक-चिह्नों का लोप हो जाता है।
समास के आवश्यक तत्त्व
(i) समास में कम-से-कम दो पदों का योग होता है।
(ii) दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो
जाते हैं। ‘एकपदी भाव’ समास है।
(iii) समास में पदों के विभक्ति-प्रत्यय लुप्त हो जाते
सन्धि और समास में अंतर
समास और सन्धि दोनों में एकीभाव होता है परन्तु दोनों में होने वाले एकीभाव अथवा एकीकरण के मध्य कुछ अन्तर होता है
जैसे(i) समास में दो पदों का योग होता है, किन्तु सन्धि
में दो वर्गों का योग होता है।
(ii) समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते
हैं, सन्धि के लिए दो वर्गों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है। इस प्रकार के मेल या विकार से समास को कोई मतलब नहीं रहता है।
(iii) सन्धि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि
समास का विग्रह किया जाता है, जैसे-पीताम्बर में दो पद हैं-पीत + अम्बर। इसका संधि विच्छेद होगा-पीत + अम्बर, जबकि इसका समास विग्रह होगा-पीत है जो अम्बर अथवा पीत है जिसका अम्बर।
द्रष्टव्य यह है कि हिन्दी में सन्धि केवल तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास संस्कृत, हिन्दी, उर्दू प्रत्येक प्रकार के शब्दों या पदों के मध्य हो जाता है, जैसे-‘राजमहल’ शब्द को लेते हैं। इसमें ‘राज’ तत्सम शब्द और ‘महल’ अरबी शब्द के मिलने से सामासिक शब्द ‘राजमहल’ बना है।
समास के प्रकार–
जिन दो शब्दों में समास होता है | उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के आधार पर समास के चार भेद किए जाते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, वह दृन्द समास कहलाता है। जिसमें कोई शब्द प्रधान नहीं होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। हिन्दी में इनके अतिरिक्त दो समास और हैं-कर्मधारय और द्रिगु ।
समास के छः भेद हैं:
अव्ययीभाव
तत्पुरुष
द्रिगु
दृन्द
बहुव्रीहि
कर्मधारय
अव्ययीभाव समास
जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद (समास) अव्यय हो जाए-वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण- प्रतिदिन, यथा-शक्ति, बेखटके आदि। इनमें पहला पद प्रति, यथा तथा बे प्रधान हैं और पूरा शब्द क्रिया-विशेषण है, यथा-दिन-दिन
तत्पुरुष समास
तत्पुरुष समास में द्वितीय पद/शब्द प्रधान होता है। साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। स्पष्ट है कि बाद वाला पद (विशेष्य) की प्रधानता रहती है। इसके पहले पद में कर्ता कारक से | यह लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों वाले पद अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं, जैसे-जलपिपासु, राज-प्रासाद, देश-गत,
आपबीती, कानाफूसी आदि।
दृन्द समास
जिस समास में सब पद प्रधान होते हैं, उसे दृन्द समास कहते हैं, जैसे-राधा-कृष्ण, घर-द्वार, गाय-बैल, चाय-पानी इत्यादि। द्वन्द्व समास का विग्रह शब्दों के मध्य और शब्द लगाकर किया जाता है अथवा द्वन्द्व सामासिक पद के मध्य और शब्द का लोप रहता है। उपर्युक्त उदाहरणों का विग्रह इस प्रकार किया जाएगा-राधा और कृष्ण, घर
और द्वार, गाय और बैल, चाय और पानी आदि।
-
बहुव्रीहि समास
जिस समास का कोई खण्ड प्रधान न हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करते समय वाला, वाली है, जिसका, जिसकी शब्द आते हैं। उदाहरणपीताम्बर। इसका विग्रह इस प्रकार होगा-पीला अम्बर है जिसका अर्थात् श्रीकृष्ण, दशानन-दश मुख हैं जिसके अर्थात् रावण,
कर्मधारय समास
जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति होती है, उसे कर्मधारय – समास कहते हैं। इसका पहला पद विशेषण होता है, जैसे-नीलकमल, नीलगाय, भलामानस,
चन्द्रमुख आदि।
द्रिगु समास
जिस समास का पहला पद संख्याबोधक हो, वह द्विगु समास कहा जाता है। उदाहरण-त्रिभुवन, त्रिलोचन, चौराहा, पसेरी, अष्टाध्यायी आदि।